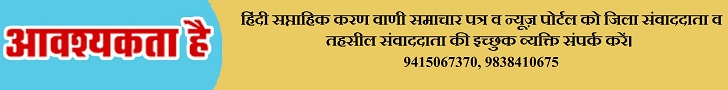दिवाली की यादें: पता नहीं कहां खो गए, समाज की देहरी पर दिया रखकर उसे रोशन रखने वाले लोग……

पंकज सिंह चौहान
पता नहीं वे उजाले की परंपराएं कहां लुप्त होती जा रही हैं, जो हर हाल में समाज में रोशनी को जिंदा रखने का जतन किया करती थीं….
बचपन में दिवाली के आते ही हम पटाखों की तरह फटने को बेताब हो जाते थे, दिमाग़ में कुछ न कुछ ख़ुरपेच सूझते ही रहते थे, उस वक़्त ये ख़ुशियां बस एक दिन की बात नही थीं, हफ़्ते भर पहले से उधम–चौकड़ी शुरू कर देते थे, आसमान की सारी रौशनी हमारी आंखों में देखी जा सकती थी, जेब खाली थी, मगर हथेली दुनियाभर की शरारतों से भरी थी।
रसोई में सदाबहार चूल्हों और देग व परातों में रखे पकवानों की ललचाने वाली गंध, घरों की सफाई–पुताई, नए कपड़ों की सिलाई, बाजारों की रौनक, खरीद–फरोख्त, बमों के धूम–धड़ाके, मेल–जोल और मस्तियों से दिवाली का रूप, रंग, गंध और स्वाद हफ्तों पहले से महसूस होने लगता था।
दिवाली का इंतजार दरअसल, दशहरे के दिन से ही शुरू हो चुका होता था। आखिरी दिन लक्ष्मी, गणेश के साथ बही–खातों, कलम–दावात, कुबेर, पंजिका व तुला पूजन और बड़ों से त्योहारी वसूलने के बाद हर ओर मिट्टी के दीयों से रोशन माहौल में छत या आंगन पर पटाखा या अनार छुड़ाते वक्त पहला ध्यान यही होता था कि अगली सुबह सबसे पहले उठना है, ताकि अधजले पटाखे कोई और चुन नहीं ले जाए।
शहर की भागम–भाग जिंदगी में किसके पास वक्त है कि कढ़ाई चढ़ाए और गर्मी में तपता रहे। लिहाजा, कोई आश्चर्य नहीं आप भी बाजार में मिलने वाले, पर घर के स्वाद से मिलने वाले व्यंजन खरीद लाए हों और जुआ–महफिलों के बजाय दोस्तों से फोन पर बात करके ही खुश हो लिए हों। दिवाली की सजावट, खरीदारी, पटाखे और पकवान अब भी हैं। बस नहीं रहा है तो दिवाली का वह उल्लास, जो बढ़ती उम्र के तकाजों ने हमसे छीन लिया है। आज के बच्चे पूजा के नाम पर हाथ भर जोड़ लें और घर में बने पकवान चख भर लें, तो गनीमत मानिए। वरना, उनकी खुशियां दोस्तों के साथ मॉल में जाने, नए ब्रैंडेड कपड़े पहनने, पिज्जा–कोक की पार्टियां करने और अनलिमिटेड फोटो खिंचवाने तक सीमित हो गई हैं। देखने को दीप और मोमबत्ती से पूरा घर जग–मग करता है, पर हम बुझे मन सेरोजाना की तरह टीवी देखकर आगंतुकों के इंतजार में दिवाली की शाम गुजारा करते हैं।‘
जब जब भी दीवाली–होली जैसे त्योहार आते हैं, वे पुरानी पीढ़ी के लोगों को अपने जमाने में ले जाते हैं, अतीत की कई स्मृतियां कौंधनेऔर कुरेदने लगती हैं, इनमें कुछ यादें खुद से, परिवार से जुड़ी होती हैं तो कुछ समाज और सामाजिक रिश्तों, रस्मों और रिवाजों से, जमाना बदलने के साथ बहुत कुछ बदला है, बदलना भी चाहिए, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन कुछ बातें, जो भले ही दशकों, शताब्दियों पुरानी हो गई हों, ऐसी होती हैं जिनका बदलना अखरता है।
समाज के सुख–दुख में साथ रहने की वे परंपराएं या तो खत्म हो गई हैं या फिर उनका क्षरण होता जा रहा है, अंधेरे को पूजने और नवाजने के इस समय में, पता नहीं वे उजाले की परंपराएं कहां लुप्त होती जा रही हैं, जो हर हाल में समाज में रोशनी को जिंदा रखने का जतन किया करती थीं, मुझे याद है, दिया रखने का यह काम केवल पास पड़ोस के घरों की देहरी पर ही नहीं होता था, बल्कि महिलाएं मंदिर के अलावा, पेड़ के नीचे, कुएं या सार्वजनिक नल पर, गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर और यहां तक की कूड़ा डालने वाली जगह के किनारे भी दिया रखकर आतीं।
जरा सोचिए, पेड़ और कुएं को भी अंधेरे में न रहने देने के पीछे कितना बड़ा दर्शन रहा होगा, हमारी वनस्पति और जल के स्रोत को अंधेरा कभी नष्ट न कर सके, नुक्कड़ का दिया राहों को हमेशा रोशन करता रहे, और कूड़ा डालने वाली जगह पर दिया रखने की बात तो कल्पनातीत है, आज स्वच्छता को एक अभियान के रूप में चलाने की बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन हमारे यहां तो कूड़ा डालने वाली जगहभी साफ और रोशन रहे, इसकी कामना और जतन किये जाते रहे हैं।
दिवाली पर समाज के हर अंधेरे के खिलाफ, प्रतीक रूप से संपन्न किए जाने वाले रोशनी के ये सारे जतन, हमारे इसी समाज में मौजूद रहे हैं, अफसोस इस बात का है कि आज रोशनी का वो मायना कहीं पीछे छूटता जा रहा है, अब बात सिर्फ अपने घरों को रोशन करने तक ही सिमट कर रह गई है, आज यदि किसी के घर दिया नहीं जलता और उसकी दहलीज अंधेरी पड़ी रहती है, तो यह उसकी ‘प्रॉब्लम’ है, समाज की देहरी पर दिया रखकर, उसे हमेशा रोशन रखने वाले लोग पता नहीं कहां खो गए हैं।